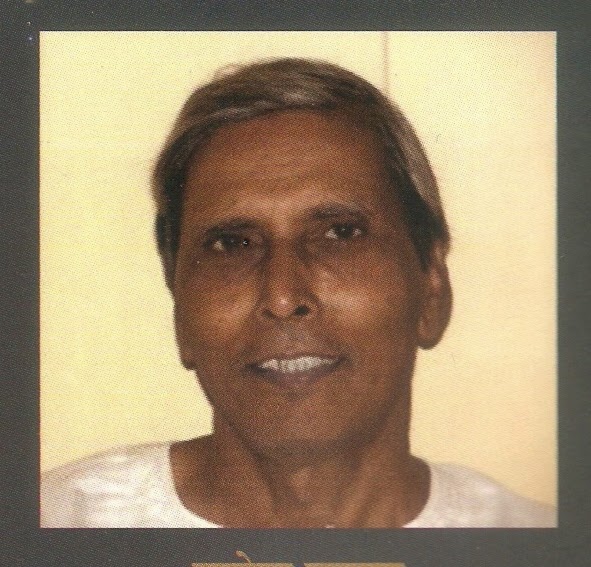.........इस गोष्ठी का विषय है- ‘मुक्तिबोध और हिंदी कविता
के पचास वर्ष’, लेकिन
मैं इस विषय पर बोलने की जगह ‘अँधेरे में और हिंदी कविता के पचास वर्ष’ पर बोलना
पसंद करूँगा | यह विषय पहले की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है | वैसे उतना छोटा भी
नहीं है कि मुझे बोलने के लिए आधे घंटे की जो अवधि दी गई है, उसमें विषय के
विस्तार को समेट सकूँ | 1964 में ‘अँधेरे में’ कविता का
प्रकाशन हुआ था और उसी वर्ष मुक्तिबोध का निधन भी हुआ | इस तरह ‘अँधेरे में’ कविता
के प्रकाशन के पचास वर्ष पूरे हो रहे हैं | इस कविता के प्रकाशन की अर्द्धशती के
अवसर पर देश में कई आयोजन हुए और उसी क्रम में आपका यह आयोजन..... इस सिलसिले का
शायद अंतिम कार्यक्रम | मुझे याद नहीं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की किसी रचना को
उसकी अर्द्धशती के अवसर पर इस तरह याद
किया गया हो | इस अर्थ में यह हिंदी की अद्वितीय रचना है | यह सौभाग्य शायद ही
किसी एक कविता को मिला हो !
‘कामायनी’ की तरह ‘अँधेरे
में’ कविता भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल है | जैसे
‘उसने कहा था’ के बिना हिंदी कहानी का कोई प्रतिनिधि संकलन नहीं तैयार किया जा
सकता, वैसे ही ‘कामायनी’ और ‘अँधेरे में’ को अलग रखकर आधुनिक हिंदी कविता पर बात
नहीं हो सकती | दूसरे कई महत्वपूर्ण कवि हैं जो कवि रूप में आधुनिक हिंदी कविता पर
चर्चा के क्रम में अवश्य ही शामिल किये जाते हैं, लेकिन उनकी कोई एक कविता चर्चा
का आधार रहे और उस काल की कविता की मुख्य प्रस्तावना भी, ऐसा संभवतः दूसरा उदहारण
देखने को नहीं मिलेगा | ‘कामायनी’ महाकाव्य है, न सिर्फ काव्य-रूप में, बल्कि अपने प्रभाव में भी; जबकि ‘अँधेरे
में’ एक लम्बी कविता भर है- लगभग 40 पृष्ठों की, लेकिन इसका प्रभाव भी वैसा ही
महाकाव्यात्मक है और युगव्यापी भी | ‘कामायनी’
आलोचकों के लिए चुनौती रही, इसलिए उसकी बहुतेरी व्याख्याएँ हुईं, उनमें से एक
व्याख्या मुक्तिबोध की भी है-‘कामायनी: एक पुनर्विचार’ नाम से | उस व्याख्या से
पता चलता है कि प्रसाद और ‘कामायनी’ का मुक्तिबोध के लिए क्या महत्व था | वे अपनी
‘सभ्यता-समीक्षा’ में ‘कामायनी’ और प्रसाद को एक बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं |
कुछ आलोचकों ने इस ओर इंगित किया है कि क्यों मुक्तिबोध आधुनिक कविता के इतिहास
में ‘कामायनी’ को इस महत्व के साथ अपने दृष्टि-पथ में रखते हैं | आखिर किसी दूसरे
कवि की रचना मुक्तिबोध के लिए वैसी चुनौती क्यों नहीं ? ‘कामायनी’ की तरह ‘अँधेरे
में’ कविता भी आलोचकों के लिए चुनौती रही है | इसकी भी अनेक
व्याख्याएं-कुव्याख्याएं हुई हैं | नामवर सिंह और रामविलास शर्मा की व्याख्याएं
ज्यादा चर्चित और बहसतलब रही हैं | एक व्याख्या नन्द किशोर नवल कि भी है, जो
फासीवाद के सन्दर्भ में इस कविता को देखती है .......मुक्तिबोध की एक व्याख्या इस
गोष्ठी के अध्यक्ष दूधनाथ सिंह की भी है | कुछ लोग कहते हैं कि वह व्याख्या किसी
काम की नहीं | लेकिन कोई बात नहीं | वह कविता पचास वर्ष बाद भी अपनी व्याख्या के
नए-नए द्वार खोलती जा रही है | यह उसके कालजयित्व और श्रेष्ठता का बड़ा प्रमाण है |
‘अँधेरे में’ ‘नई कविता’
की सबसे बड़ी उपलब्धि है | वह न सिर्फ ‘नई कविता’ की, बल्कि सम्पूर्ण छायावादोत्तर
दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि है | वह ‘कामायनी’ और ‘राम की शक्ति पूजा’ के बाद हिंदी
की सबसे महान कविता है | महत्वपूर्ण और बड़ी कविताएँ अनेक हैं, अनेक प्रगतिशील और
गैर प्रगतिशील कवि भी हैं, हिंदी कविता के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ‘अँधेरे में’ के मुकाबले किसी दूसरी
कविता को नहीं रखा जा सकता | यह अपना उदाहरण अपने आप है | नई कविता दौर की ही एक
महत्वपूर्ण उपलब्धि अज्ञेय की लम्बी कविता ‘असाध्य वीणा’ भी है | वह भी महत्वपूर्ण
कविता है | उसके भी अनेक पाठ-कुपाठ हुए हैं | एक कुपाठ नामवर सिंह का भी है | ‘कविता
के नए प्रतिमान’ में ‘असाध्य वीणा’ की जो व्याख्या है, उससे आप परचित होंगे | उस कविता का सब कुछ नामवर सिंह के लिए ‘बासी’
है | रामविलास जी को तो उसमें नव रहस्यवाद नजर आया | लेकिन आज जब मैं उस कविता को
पढ़ता हूँ तो इन कुपाठों से अलग वह एक सुन्दर और महत्वपूर्ण कविता के रूप में मुझे
दिखाई देती है | यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने
अज्ञेय का विरोध जरूर किया, लेकिन उन्हें अछूत नहीं माना | इस तथ्य की ओर ध्यान
देने की जरूरत है कि मुक्तिबोध की विरासत को संभालने का दावा करने वाली जो नई पीढ़ी
है वह अपने ‘विरोधी’ विचार के कवि-लेखक को पढ़ती ही नहीं | सुने-सुनाये आधारों पर
बयान देने और हमले करने का प्रचलन इधर के दौर में ज्यादा बढ़ा है........बहरहाल एक
ही दौर में लिखी गयी दो बड़ी कविताएँ हैं- ‘अँधेरे में’ और ‘असाध्य वीणा’ | एक में
जगत-समीक्षा है तो दूसरी में कला-समीक्षा | एक अपने समय की तमाम उथल-पुथल को समेटे
हुए है तो दूसरे में कला-साधना का समाधि-भाव है | मैं अनावश्यक रूप से दोनों
कवियों और कविताओं की तुलना करके एक को
श्रेष्ठतर और दूसरे को कमतर, परीक्षोपयोगी मूल्यांकन प्रणाली वाली समीक्षा के
विरुद्ध हूँ......फिर भी दोनों के बारे में मेरी राय जानना चाहें तो मैं कहना
चाहूँगा कि ‘अँधेरे में’ मेरी लिए ऐसी कविता है, जिसे मैं जीवन भर बार-बार पढ़ना
चाहूँगा |
आज जब हम ‘अँधेरे में और
हिंदी कविता के पचास वर्ष’ पर बात कर हैं तो कुछ बातें साफ़ हो जानी चाहिए | ‘अँधेरे
में’ कविता जब लिखी गयी थी तब वह शीतयुद्ध का समय था | दुनिया दो खेमों में बंटी
हुई थी | समाजवादी खेमा और गैर समाजवादी खेमा | हिंदी में भी दो ध्रुव थे-प्रगतिशील
और गैरप्रगतिशील | मुक्तिबोध के सामने
पक्ष बिलकुल साफ़ था | वे विश्वस्तर पर समाजवादी खेमे के पक्ष में थे | हिंदी में प्रगतिशील चेतना के पक्ष में अपने पक्ष को
लेकर मुक्तिबोध के सामने कोई दुविधा नहीं थी | वे बड़े मजे में पूछ सकते थे कि
‘पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है ?’, इस पक्ष में हो कि उस पक्ष में ? आज
सोवियत संघ समेत तमाम समाजवादी मुल्क बिखर चुकें हैं, दुनिया दो ध्रुवीय न रहकर एक
ध्रुवीय हो गयी है | वैसे में आज कवि को अपना पक्ष बनाने में मुक्तिबोध के समय से
अधिक सतर्कता और सचेतता की जरुरत है | यह समस्या मुक्तिबोध के सामने नहीं रही होगी
| भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन बिखराव और हताशा के दौर से गुजर रहा है | वह भारतीय
युवा वर्ग को आकर्षित करने और उसके भीतर मानव-मुक्ति का नया स्वप्न जगाने में उस तरह कारगर नहीं है | आज
कम्युनिस्ट होना मुक्तिबोध के समय की तरह अग्निपथ पर चलने की तरह भी नहीं है | इसलिए
आज के कवि के सामने वे चुनौतियां भी नहीं हैं, जो मुक्तिबोध के सामने थीं |
इस कविता के अपने ऊपर प्रभाव
की चर्चा करूँ तो मैं कहना पसंद करूँगा कि इसका प्रभाव मेरे ऊपर वैसा ही पड़ता है
जिस तरह कबीर, सूर, रैदास, तुलसी, नानक, मीरा आदि भक्त कवियों को पढ़ने पर पड़ता है
| ‘अँधेरे में’ की विषयवस्तु भक्ति विषयक नहीं है | वह हमारे समय के झंझावातों की
कविता है | उसका प्रभाव मेरे ऊपर अगर भक्ति कविता की तरह पड़ता है तो इस अर्थ में
नहीं कि मुझे उससे कोई धार्मिक-आध्यात्मिक चेतना और तोष प्राप्त होता है, बल्कि
इसलिए कि भक्ति-कविता में जो शब्द और कर्म की नैतिक आभा है, वह आभा मुझे यहाँ भी
दिखाई देती है | भक्ति कविता को पढ़ते हुए कवि के शब्द और कर्म में हम कोई द्वैत
नहीं पाते, मुझे ‘अँधेरे में’ को पढ़ते हुए उसी भाव-भूमि की अनुभूति होती है | ‘अँधेरे
में’ मेरे लिए छायावादोत्तर युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो इसकी एक वजह और है | वह
यह कि यह कविता सिर्फ दिमाग की ही नहीं, दिल की भी बेचैनी के साथ पाठक के सामने
उपस्थिति होती है | इसी के साथ यह कि ‘करुण रसाल और ह्रदय’ के संयोग से बनी इस
कविता का स्वर छायावादोत्तर दौर का सबसे भिन्न और पाठकीय भरोसे का स्वर है | यह
बेचैनी एक लय की तरह पूरी कविता में व्याप्त है | यह बेचैनी किसी भावुक प्रसंग की
नहीं, गहन-गंभीर विचार की है, जो संगीत की तरह पूरी कविता में सुनाई देती है | मुक्तिबोध
कहते हैं ‘आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी / मेरी नींद गँवा दी’, तो यूँ ही नहीं
कहते | यह चैन भुलाने और नींद गंवाने की भाव-भूमि से पैदा हुई कविता है | यह कविता
सिर्फ विचार से नहीं पैदा हुई है | विचार के साथ हृदयपक्ष भी जुड़ा है- ‘करुण रसाल
वे ह्रदय के स्वर हैं’| विचार के साथ ‘ह्रदय के स्वर’ इस कविता की शिराओं में अपनी पूरी गति और
ऊष्मा से भरे हुए हैं | यह इसका सबसे मजबूत पक्ष है |
मुक्तिबोध की यह कविता
मुझे इसलिए भी प्रिय है कि उसमें गीतात्मक अनुगूँज है | इसके कारण इसमें गजब का
प्रवाह है | गीतात्मक अनुगूँज कहीं प्रकट
होकर तो कहीं लय बनकर पूरी कविता में व्याप्त है | बानगी के तौर पर कुछ पंक्तियाँ
देखी जा सकती हैं -
अब युग बदला है वाकई
कहीं आग लग गई,कहीं गोली चल गई
भागता मैं दम छोड़
घूम गया कई मोड़
ओ मेरे आदर्शवादी मन
ओ मेरे सिद्धांतवादी मन
हाय-हाय नुमा,टॉलस्टॉय नुमा
‘अँधेरे में’ कविता अपने जटिल वितान के बावजूद ऐसा बहुत कुछ कहती है जो बहुत
सहज ढंग से सिद्धांत-सूत्र की तरह आदर्श वाक्य के रूप में नई पीढ़ी की जुबान पर है |
किसी कविता का इस तरह सिद्धांत वाक्य बनकर जन-समाज में लोकप्रिय होना मामूली बात
नहीं है | यह भूमिका वही कविता अदा करती है, जो जीवन की आग से पैदा होती है | कुछ
उदहारण देखे जा सकते हैं-
कविता में कहने की आदत नहीं,पर कह दूँ
वर्तमान समाज चल नहीं सकता|
पूँजी से जुड़ा हुआ ह्रदय,बदल नहीं सकता|
स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी
छल नहीं सकता मुक्ति के मन को
जन को |
दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर
दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट
कोई भी मुर्गा
यदि बांग दे उठे जोरदार
बन जाए मसीहा
अभिव्यक्ति के खतरे
उठाने ही होंगे
तोड़ने होंगे ही गढ़ और मठ सब
हिंदी कविता का कौन-सा प्रेमी पाठक मुक्तिबोध की ऐसी पंक्तियों को दुहराता न
मिलेगा !
‘अँधेरे में’ कविता का एक और
वैशिष्ट्य मुझे बार-बार आकर्षित करता है | वह है, उसका नाटकीयता से भरपूर रचाव | एक-एक
पंक्ति नाटक के संवाद की तरह कसी हुई है और किसी नाटक के संवाद की तरह प्रभाव
डालती है | नाटक के दृश्यों की ही तरह ‘अँधेरे में’ के दृश्य बदलते हैं | प्रसाद
के नाटकों की संवाद-योजना से ‘अँधेरे में’ की नाटकीयता का मिलान करके इसको देखा जा
सकता है | जिन्होंने ‘अँधेरे में’ कविता का नाट्य मंचन देखा है, वे उसके
नाट्यधर्मी प्रभाव के कायल हुए बिना नहीं रहेंगे :
खुला-खुला कमरा है, सांवली हवा है
झांकते हैं खिड़की से, अँधेरे में टंके हुए सितारे
फैली है बर्फीली साँस-सी, वीरान
तितर-बितर सब फैला है सामान
इस कविता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट हो
जाता है कि मुक्तिबोध को देश में मार्शल लॉ का खतरा उपस्थित होता हुआ दिखाई दे रहा
था | वे उस स्थिति की भी कल्पना कर रहे थें, जिसमें दिन के उजाले में जन-समर्थन का
स्वांग करने वाले लोग रात के अँधेरे में मार्शल लॉ के समर्थन में थे | मुक्तिबोध के
सामने जनता की मुक्ति की एक ही राह थी और वह थी- जनक्रांति | ‘अँधेरे में’ कविता
उस जनक्रांति के स्वप्न की कविता है | वह जनक्रांति बहुत कुछ बोल्शेविक क्रांति का
समरूप है | आज वैसी जनक्रांति की बात न कोई करता है और न उसकी गूँज इधर की कविता
में सुनाई पड़ती है | अब कविता में प्रतिरोध का जनक्रांति वाला स्वर नहीं है | प्रतिरोध
के अब अनेक मंच हैं और अनेक तरह के स्वर हैं | अब दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक
अपने प्रतिरोध को कविता में वैसे नहीं दर्ज करते जिसे ‘अँधेरे में’ की स्पष्ट
विरासत कहा जाए | अनामिका ‘दरवाजा’ शीर्षक कविता में कहती हैं :
मैं एक दरवाजा थी
मुझे जितना पीटा गया
मैं उतना ही खुलती गई|
अन्दर आए आनेवाले तो देखा-
चल रहा है एक वृहत्चक्र- चक्की रूकती है तो चरखा चलता है
चरखा रुकता है तो चलती है कैंची- सुई
गरज यह कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ-कुछ !
.........और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू
तारे बुहारती हुई बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर-
सृष्टि के सब टूटे- बिखरे कतरे जो
एक टोकरी में जमा करती जाती है
मन की दुछत्ती पर |
यह काव्य-स्वर ‘अँधेरे में’ कविता से अलग हिंदी कविता में एक नए प्रस्थान की
तरह है | मुक्ति का स्वप्न तो इसमें भी है | इसी तरह गगन गिल ‘अँधेरे में बुद्ध’
सीरीज की कवितायें जब लिखती हैं तो स्त्री-मुक्ति का नया ही सन्दर्भ उभरता है |
‘यह आकांक्षा समय नहीं’ संग्रह में उनकी एक कविता है ‘वह सचमुच’ | उसे भी जरा
देखिए :
दरवाजा भड़भड़ा रहा है
जाने कब से
घंटी बज रही है
फोन की
तुम्हारे खाली कमरे में
तुम्हारी खिड़की के बाहर
पिछले कई दिन-रात से
मंडरा रही है
तुम्हारी सोई आँखों के पास
देख रही है
निकाल कर
तुम्हारा दिल
रोक रही है रास्ता
पकड़ कर तुम्हारा चीवर
मैं तुम्हे जाने नहीं दूंगी
मैं तुम्हे जाने नहीं दूंगी
वह
सचमुच आन पहुंची है
तुम्हारे एकांत में
दलित कवयित्री रजनी अनुरागी की मुक्ति
का स्वप्न कुछ दूसरा है-
अगर पढ़ सको तो पढ़ो
हमको ही
हमारी कविता की तरह
हम औरतें भी
एक कविता ही तो हैं |
अँधेरे में से आगे और उससे अलग हिंदी कविता का यह नया इलाका है | एकदम नया और
उर्वर | मुक्ति को नया अर्थ देता हुआ | हिंदी कविता के आकाश में नए क्षितिज को
उद्घाटित करता हुआ | मुक्ति का यह सपना ‘अँधेरे में’ के स्वप्न का विस्तार है या
कुछ अलग है, इसपर विचार होना चाहिए |
मुक्तिबोध की चेतना जिस विचारधारा से संचालित है, जनक्रांति उसकी अनिवार्य
परिणति है | भविष्य में जनक्रांति होगी और जनता की मुक्ति की सारी बाधाएं दूर हो
जाएंगी, इसे लेकर ‘अँधेरे में’ कविता के रचनाकार को कोई दुविधा नहीं है | उस जमाने
में विश्वस्तर पर और भारतीय समाज में मार्क्सवाद की जो मोहक उपस्थिति थी, उसे
देखते हुए मुक्तिबोध के जनक्रांति के सपने को यथार्थ मानने में तब भला किसे आपत्ति
हो सकती थी ! लेकिन पचास वर्षों बाद दुनिया और भारत के नक़्शे पर जनक्रांति का
आदर्श कहीं भी मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं पड़ता | इसलिए आज न तो उनका जनक्रांति
का वह सपना निर्विवाद है और न उस जनक्रांति के लिए लड़ने वाले जन की निष्ठा |
मुक्तिबोध आज होते तो उनकी जनक्रांति के सपने को कई ओर से चुनौतियां मिलतीं | कारण
साफ़ है- आज शोषक और शोषित के विभाजन की स्वीकार्यता निर्विवाद नहीं है | प्रगतिशील
मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा का यथार्थ और वर्ग का आग्रह ब्राह्मणवादी करार
दिया जा चुका है | नागार्जुन की कविता ‘हरिजन गाथा’ का विरोध दलित विमर्शकारों
द्वारा किया जा चुका है | ‘सरस्वती’ में हीरा डोम की कविता ‘अछूत की शिकायत’ के
प्रकाशन को महावीर प्रसाद द्विवेदी का षडयंत्र बताया जा चुका है, आदि-आदि | ऐसे
में ‘अँधेरे में’ के सामने का जो काव्य-परिदृश्य है उसमें बहुत बदलाव आया है | यह
बदलाव लाने में स्त्रियों की भूमिका तो है ही, दलित कवियों की भी भूमिका है |
......मैंने पहले कहा कि ‘अँधेरे में’ में भारतीय जन के प्रतिरोध का जो का दृढ
स्वर है और जनक्रांति का जो सपना है उसे हमारे दौर की अस्मितावादी प्रतिरोधी
आवाजें उस रूप में स्वीकार नहीं करतीं, उन्हें मुक्ति की समाजवादी क्रांति के बदले अपनी-अपनी मुक्ति का सवाल
ज्यादा परेशान करता है | ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है- ‘ठाकुर का कुआँ’ | यह
प्रेमचंद की कहानी का कविता में दलित पाठ है-
चूल्हा मिट्टी का
मिट्टी तालाब की
तालाब ठाकुर का
रोटी बाजरे की
बाजरा खेत का
खेत ठाकुर का
बैल ठाकुर का हल ठाकुर का
हल की मुठ पर हथेली अपनी
फसल ठाकुर की
कुआँ ठाकुर का
खेत खलिहान ठाकुर के
फिर अपना क्या?
गाँव?
शहर?
देश ?
इस कविता का कैनवास निश्चित रूप से ‘अँधेरे में’ जैसा बड़ा
नहीं, बहुत छोटा है | प्रश्न है कि इसके भीतर उठने वाले सवाल दलित जीवन के सन्दर्भ
में बड़े हैं या नहीं ? यह ‘अँधेरे में’ जैसी जटिल वितान वाली कविता के सामने
सीधी-सपाट है, लेकिन दलित भारत की ओर से सवाल तो ऐसी ही कविताएँ उठाती हैं | जय
प्रकाश कर्दम की एक कविता है- ‘किले’ |
उसका एक अंश है –
ब्राम्हण का मान
ठाकुर की शान
सेठ की तिजोरी
खेत-खलिहान
मिल-कारखाने
कोठी और हवेली मेरे श्रम और शोषण से
फले-फूले हैं
..............
असमानता और अन्याय के
ये सारे किले मेरी
आँखों में गड़े हैं |
ये दलित कविताएँ एक बयान की तरह हैं- सरल और सपाट | रेटोरिक
से भरी हुई | हिंदी कविता भाव और शिल्प की जिस ऊंचाई पर पहुँच चुकी है, उसे देखते
हुए ये बयानधर्मी कविताएँ कविता के परिभाषित परिसर की नहीं लगतीं | खुद अँधेरे में कविता के जरिए
हिंदी कविता का आकाश जितना विस्तृत और ऊँचा हुआ है उसे देखते हुए इन्हें सरल
कविताओं के खाते में डाला जा सकता है, लेकिन इसमें उठने वाले सवाल हिंदी कविता में
बिलकुल नए हैं | इन नए सवालों से बनने वाली हिंदी कविता चाहे जितनी सरल-सपाट लगे
वह ‘अँधेरे में’ के आगे हिंदी कविता की नई ज़मीन है इससे कौन इनकार करेगा ! भले वह
भूमि अभी थोड़ी अनुर्वर और उबड़-खाबड़ ही सही |
‘अँधेरे में’ से पता चलता है कि मुक्तिबोध ने प्रगतिशील हिंदी कविता का अलग
रास्ता पकड़ा | वह रास्ता नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रगतिशील कवियों से
भिन्न था | वे ‘नई कविता’ के भीतर ही प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना का संघर्ष कर
रहे थे | कामरेड डांगे के नाम उनका जो ऐतिहासिक पत्र है वह इसका प्रमाण है |
मुक्तिबोध ने समाज और विचारधारा के साथ व्यक्ति के ह्रदय पक्ष को जोड़ा | हृदय-पक्ष
यानी व्यक्ति का अनुभव, द्वंद्व, आत्मसंघर्ष आदि | विचारधारा के साथ उनकी आत्मा के
दर्पण पर पड़ने वाले अनुभव के प्रकाश से यह कविता निर्मित होती है | उन्होंने उभरते
हुए नए मध्यवर्ग की शक्ति को पहचाना, उन्होंने यह भी देखा कि इस वर्ग की कथनी और
करनी में द्वैत है | मध्यवर्गीय व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने मुक्तिकामी संघर्ष
का आकलन किया और एक आदर्श जनवादी व्यक्ति की तस्वीर पेश की, जिसका चरम उद्देश्य
है-अभिव्यक्ति के पूर्ण रूप की खोज | लेकिन अँधेरे में’ के आगे हिंदी कविता का जो
प्रगतिशील-जनवादी परिदृश्य है, उसमें आत्मा का आयतन कम वैचारिक चेतना का आयतन
ज्यादा प्रमुख है | इस लिहाज से मैं आलोकधन्वा, राजेश जोशी और अरुण कमल की कविताओं
को उदाहरण रूप में रखना चाहूँगा | ‘मैं’
इन कविताओं में भी है, लेकिन यह ‘अँधेरे में’ के ‘मैं’ से अलग लगता है | आलोकधन्वा
की कविता ‘जनता का आदमी’ की कुछ पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं –
जब कविता के वर्जित प्रदेश में
मैं एकबारगी कई करोड़ आदमियों के साथ घुसा
तो उन तमाम कवियों को
मेरा आना एक अश्लील उत्पात-सा लगा
जो केवल अपनी सुविधा के लिए
अफीम के पानी में अगले रविवार को चुरा लेना चाहते थे
अब मेरी कविता एक ली जा रही जान की तरह बुलाती है,
भाषा और लय के बिना,केवल अर्थ में-
उस गर्भवती औरत के साथ
जिसकी नाभि में सिर्फ इसलिए गोली मार दी गयी
कि कहीं एक और ईमानदार आदमी पैदा न हो जाए |
कुछ लोगों ने ‘जानता का आदमी’ को ‘अँधेरे में’ के बाद सबसे
महत्वपूर्ण कविता घोषित किया था | इस कविता का जितना शोर एक ज़माने में था, आज उसका
अता-पता नहीं है | उसका कारण यह है कि इस कविता का प्रपेक्षण बिंदु ही जनक्रांति
का किताबी आइडिया है, जिसका कवि के जीवनानुभव से कुछ लेना-देना नहीं है | यह
वैचारिक चेतना से संचालित है जिसमें ‘अँधेरे में’ जैसा ईमानदार आत्मालोचन का अभाव
है | ‘जानता का आदमी की तुलना में आलोक की ‘पतंग’ और ‘कपड़े के जूते’ अधिक
विश्वसनीय और प्रभावशाली कविताएँ हैं | ‘जनता का आदमी’ के साथ ही बहुतेरी ऐसी
कविताएँ उस दौर में लिखी गई जो थोड़े दिन के शोर-शराबे के बाद सतह पर बैठ गईं | अब
इससे अलग राजेश जोशी की एक कविता ‘मै झुकता हूँ’ को देखते हैं, जिसमे मध्यवर्गीय
व्यक्ति की चापलूसी और चालाकी पर चोट है | मानवीय गरिमा को स्वाभिमान दिलाने के
क्रम में राजेश जोशी लिखते हैं -
दरवाजे से बाहर जाने से पहले
अपने जूतों के तस्में बाँधने के लिए मैं झुकता हूँ
रोटी का कौर तोड़ने और खाने
झुकता हूँ अपनी थाली पर
जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ|
झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं
जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है
किसी शक्तिशाली के सामने
जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आखें
झुकता हूँ
जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आँखें झुकती हैं
आलोकधन्वा और राजेश जोशी की कविताओं के साथ अरुण कमल की
‘अंत’ शीर्षक कविता को भी इसी क्रम में
देखा जा सकता है –
आखिर इसी जान
इसी देह की खातिर तो सब किया
जहाँ बोलना था चुप रहा
जिससे बोलना बंद कर देना था उससे
हँस-हँस कर बोला
आखिर इसी देह की खातिर
नाक पर डाले रुमाल
गरीब बहन के आँगन से गुजरा
और बलवंत के आगे टांगे रहा भरा पीकदान
‘अँधेरे में’ और मुक्तिबोध की जो जनवादी काव्य-परंपरा है,
ये कवि उसी परंपरा के माने जाते हैं | इन कवियों की जो तीन कविताएँ यहाँ रखी गई
हैं, इन तीनो कविताओं में ‘मैं’ है, जो पाठक से संवाद करता दिखाई पड़ रहा है | क्या
इन कविताओं का ‘मैं’ ‘अँधेरे में’ के ‘मैं’ से तुलनीय है ? ‘अँधेरे में’ कविता में
जगत समीक्षा और आत्म समीक्षा का जो द्वंद्व है, वह क्या इनमें है ? ‘अँधेरे में’
के ‘मैं’ के भीतर जो द्वंद्व और तनाव है, वह इनमें कम है | कहना ही हो तो मैं कहना
चाहूँगा कि ‘अंत’ का जो ‘मैं’ है वह पाठक को ज्यादा भरोसे का लगता है | ‘मैं झुकता
हूँ’ और ‘जानता का आदमी’ का स्थान क्रमशः उसके बाद होगा | मुक्तिबोध ‘नई कविता का
आत्मसंघर्ष’ नामक अपने प्रसिद्ध निबंध में अपने समय की कविता का ‘अपने परिवेश के
साथ द्वंद्व स्थिति’ अनिवार्य मानते हैं और कवि के लिए उन द्वंद्वों का अध्ययन
जरुरी समझते हैं | क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके समय की कविता ‘पुराने
काव्य-युगों से कहीं अधिक, बहुत अधिक, अपने परिवेश के साथ द्वंद्व स्थिति में
प्रस्तुत है | इसलिए उसके भीतर तनाव का वातावरण है |’ पाब्लो नेरुदा अपने
‘मेम्वायर्स’ में कविता के लिए ‘रियल’ और ‘अनरिअल’ के बीच तनाव और द्वंद्व की
उपस्थिति को ज्यादा ठीक मानते हैं |
लेकिन प्रश्न है कि ‘अँधेरे में’ को उसके बाद की
प्रगतिशील-जनवादी कविता का निकष क्यों बनाया जाए ? मुक्तिबोध के समय का न तो
विश्वव्यापी-राष्ट्रव्यापी वैसा राजनीतिक माहौल है और न सपनो-आदर्शों से
अनुप्रमाणित मुक्तिबोध सरीखी पीढ़ी | ‘अँधेरे में’ कविता जिस यूटोपिया,
सामजिक-राजनीतिक संघर्ष और आत्म संघर्ष की उपज है, जितने विस्तृत एवं जटिल वितान
तथा ताने-बाने की रचना है, वह उसे महाख्यानपरक कविता के दर्जे में बिठाता है | वह कविता
अंतर्वस्तु के स्तर पर बहुस्तरीय तथा शिल्प एवं काव्यभाषा के स्तर पर बहुआयामी है
| इसमें भाषा, भाव और शिल्प के बहुतेरे उतार-चढ़ाव हैं | यह एक सम पर चलने वाली
कविता नहीं है, जैसे कि ‘असाध्य वीणा’ | यथार्थ और फैंटेसी तथा स्वप्न और जागृति
के धरातल पर यह एक साथ चलती है | इतने जटिल वितान और ‘विजन’ की कविता हर दौर में
लिखी ही जाए, कोई जरुरी नहीं | इसका अनुकरण तो हरगिज संभव नहीं, प्रभाव की कुछ
छायाएँ भले ही कहीं-कहीं दीख जाएँ | इस अर्थ में मुक्तिबोध ‘निरबंसिया’ कवि हैं |
बाद की पीढ़ी पर ‘अँधेरे में’ का प्रभाव कितना है, यह तो विस्तृत छानबीन का विषय
है, लेकिन इतना तय है कि बाद की हिंदी कविता ‘अँधेरे में’ की तत्सम बहुलता से
मुक्त हो गई | यह मुक्ति जरुरी थी |
‘अँधेरे में’ कविता को पढ़ते हुए एक बात से मैं थोड़ा हैरान
हुआ | मुक्तिबोध इसमें तोल्स्तोय, तिलक और गांधी का बड़ा ही सकारात्मक स्मरण करते
हैं | १९६० के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के आइकन तो ये हर्गिज नहीं थे | तोलस्ताय को लेनिन ने ‘सोवियत
क्रांति का दर्पण’ जरुर कहा था | इसलिए उनके प्रति सम्मान तो था, लेकिन आइकन तो
गोर्की थे | कम्युनिस्ट पार्टी का नजरिया गांधी के प्रति ही काफी कठोर था, तिलक की
तो खैर बात ही छोड़िए ! ऐसे में इन तीनों के स्मरण का अर्थ क्या है ? लगता है तब
कम्युनिस्ट पार्टी की जो लाइन थी, मुक्तिबोध उसका अतिक्रमण करते हैं | ऐसा करके
क्या वे तब की मार्क्सवादी समझ को अद्यतन कर रहे थे ? एक बात और ध्यान देने लायक
है- ‘अँधेरे में’ का प्रकाशन ‘कल्पना’ में हुआ था | ‘कल्पना’ समाजवादियों की
पत्रिका थी | उसके प्रेरणा-पुरुष राममनोहर लोहिया थे और संचालक उनके समाजवादी सखा
बदरीविशाल पित्ती | संपादक मंडल में प्रायः समाजवादी लोग ही थे | मुक्तिबोध का
मार्क्सवादी रुझान जगजाहिर था | कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के
अपने-अपने विवाद भी थे | फिर भी ‘कल्पना’ ने व्यापक वामपंथी समझ का परिचय देते हुए
मुक्तिबोध समेत किसी भी मार्क्सवादी कवि-लेखक को छापने से परहेज नहीं किया | मेरी
सहज जिज्ञासा है कि तब मार्क्सवादी मंचों से निकलने वाली पत्रिकाएं भी इसी उदारता
और व्यापक समझ के तहत समाजवादी लेखकों को छापती थीं या नहीं ? मुझे लगता है कि तब
की बात तब के लोग जानें, लेकिन आज भी मार्क्सवादी मंचों की पत्रिकाओं में यह
उदारता और खुलापन नहीं आया है | जिस परम अभिव्यक्ति की खोज करते हुए मुक्तिबोध ने
‘अँधेरे में’ कविता लिखी थी, उस अभिव्यक्ति पर तब की तुलना में आज कई गुणा अधिक
खतरा है | ऐसे वक्त में यह कविता व्यापक लोकतान्त्रिक और वामपंथी (अगर वामपंथ
सिर्फ कम्युनिस्ट संगठनों तक महदूद नहीं है तो) समझ और पहल की मांग करती है |
........... ‘अँधेरे में और हिंदी कविता के पचास वर्ष’ पर बात करते हुए अपनी कुछ
समझ, कुछ ऊहापोह को इस तरह मैंने आपसे साझा किया | अपनी समझ से कुछ आयामों पर
मैंने बात की | संभव है कुछ आयाम और भी हों, जिनपर आगे बातचीत होगी .............
(म. गाँ. अं. हि. वि. वि., वर्धा के इलाहाबाद केंद्र द्वारा
२९ दिसंबर २०१४ को आयोजित गोष्ठी में दिए गए वक्तव्य का लिखित एवं किंचित
सम्पादित-संवर्धित रूप)
प्रस्तुति :
सुनील कुमार मिश्र